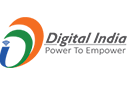25-02-2025 : उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल महोदय का उद्बोधन ।
जय हिन्द!
पर्वतराज हिमालय क्षेत्र से शुरु हुए आयुर्वेद के ज्ञान गंगा के प्रवाह की परंपरा को आगे बढ़ा रहे प्रतिष्ठित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 100 वर्ष से अधिक पुराने ऋषिकुल परिसर के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में आपके मध्य उपस्थित होने पर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।
आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं, डिग्री प्राप्त करने वाले सभी स्नातक, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई देता हूँ। मैं राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ।
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा प्रणाली के गौरवशाली अतीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। यह भी आवश्यक है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ें और इसे एक प्रमाण आधारित चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करें।
प्रिय शिक्षार्थियों,
आप सभी इस प्राचीन भारतीय महान परंपरा के वाहक हैं। आप केवल एक पेशेवर चिकित्सक ही नहीं बल्कि समाज को स्वस्थ और निरोगी रखने वाले अग्रदूत भी हैं। आज जो लोग डिग्री प्राप्त कर रहें हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप आयुर्वेद के उत्थान में अपना सशक्त योगदान देंगे, जिससे कि इस प्राचीन ज्ञान से पूरा विश्व लाभान्वित हो सके।
हिमालय का यह आँगन देवभूमि उत्तराखण्ड, ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र ही नहीं है अपितु चेतना के उत्थान की समृद्ध परंपरा का वाहक है। इन अदभुत पर्वतों से ही ब्रह्मांड के निर्माता ने मानव जाति के कल्याण के लिए ऋषियों को उपचार का यह समग्र ज्ञान दिया। ब्रह्मा के मुख से अवतरित आयुर्वेद के ज्ञान को भगवान इन्द्र ने ऋषि भारद्वाज के माध्यम से धरती पर प्रचारित व प्रसारित करने का जो पुण्य कार्य किया वह अद्वितीय है।
आयुर्वेद विश्व को भारत की अमूल्य देन है। भगवान धन्वंतरि को जहां आयुर्वेद का जनक माना जाता है वहीं चरक को औषधि-शास्त्र एवं सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है। आयुर्वेद, दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर बल दिया जाता है।
आयुर्वेद का हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अपने आस-पास के पेड़ पौधों नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन, अश्वगंधा का हम सब ने कभी न कभी औषधि के रूप में उपयोग किया ही होगा। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे-जैसे समाज में आधुनिकता बढ़ती गई, हम प्रकृति से दूर होते गए, इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना हम छोड़ते गए। लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और हमारी यह प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, आज जन-जन में लोकप्रिय हो रही है।
साथियों,
हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के मुख्य स्रोत जड़ी-बूटी और वनस्पति होते हैं। इसलिए आयुर्वेद का विकास न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। कई पेड़-पौधे इसलिए विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम उनकी महत्ता को जानेंगे तभी हम उनका संरक्षण भी करेंगे। इसलिए हमें वनस्पतियों की महत्ता को समझते हुए इनके संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है।
हम जानते हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवनशैली है। यह हमें केवल रोगों से मुक्ति नहीं, बल्कि स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। हमारे ऋषियों और वैद्यों ने सैकड़ों वर्ष पहले जो ज्ञान अर्जित किया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रभावी है।
आयुर्वेद का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मनुष्य रोगी न बने। इसके सिद्धांतों और उपचार में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जो इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और सतत विकास के लिए उपयुक्त बनाता है। आयुर्वेद में विभिन्न प्राकृतिक औषधियों और उपचार विधियों के माध्यम से संक्रमण से लड़ने की शक्ति होती है जो बिना किसी हानिकारक प्रभाव के रोग निरोधी गुण प्रदान करती हैं।
साथियों,
आयुर्वेदिक चिकित्सा शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। जो न केवल लक्षणों को शान्त करता है, बल्कि रोगों के मूल कारणों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में शरीर की संरचना, दोष, वात पित्त, कफ के प्रकोप और विभिन्न रोगों के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है।
आज आधुनिक शोध भी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ और चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावशीलता सिद्ध कर रहे हैं।
जीवन शैली संबंधी रोग, जैसे मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, को नियंत्रित करने में आयुर्वेदिक आहार, जड़ी बूटियाँ और योग कारगर सिद्ध हो रहे हैं।
आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान परंपरा और नवाचार का संगम है। यदि इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए तो यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रभावशाली चिकित्सा प्रणाली बन सकती है।
योग, पंचकर्म, आयुर्वेदिक औषधियाँ, और नाड़ी परीक्षण जैसी विधियाँ अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही हैं।
वर्तमान युग में जहाँ पर्यावरणीय असंतुलन, मानसिक तनाव, महामारी और एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, वहां आयुर्वेद के सिद्धांत एक स्थायी और समग्र समाधान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए गुणवत्ता मानकों का पालन, वैज्ञानिक प्रमाण और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ समन्वय आवश्यक है।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को शान्त करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी कारगर है। प्रकृति आधारित चिकित्सा प्रणाली जिसमें जड़ी बूटियाँ और जैविक उत्पादों का उपयोग किया जाता है इसके दुष्प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम हैं।
साथियों,
अच्छे चिकित्सकों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी प्रयास गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। औषधीय जड़ी-बूटियों एवं वनस्पतियों की मांग में वृद्धि से किसानों की आय भी बढ़ेगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में आयुर्वेद का सशक्त योगदान हो, इसके लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। आयुर्वेद का पुनरुत्थान तभी संभव है जब इसे वैज्ञानिक प्रमाणों आधुनिक अनुसंधान और नवाचार के साथ जोड़ा जाए। शोध संस्थानों और चिकित्सा समुदाय के सहयोग से इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। आज जब पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा और होलिस्टिक हीलिंग की ओर अग्रसर हो रही है तब भारत के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकते हैं।
किसी भी चिकित्सा पद्धति के प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर रिसर्च और इनोवेशन आवश्यक है। आयुर्वेद में सदियों तक निरंतर नए-नए प्रयोग होते रहे हैं। औषधियाँ प्रायः पेड़-पौधों और पशु-उत्पाद से बनती थीं। आज समय की मांग है कि आयुर्वेदिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों जिससे उनका निर्यात किया जा सके। इसके लिए आवश्यकता है कि हम आयुर्वेद के अपने ज्ञान के भंडार को एविडेंस बेस्ड और साईंटिफिक एप्रोच के साथ विश्व-स्तर पर मान्यता दिलाने में सफल हों।
खान-पान की गड़बड़ी, असंतुलित जीवन-शैली, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण नए-नए रोग पैदा हो रहे हैं। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता तथा उनके रोकथाम में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पूरे विश्व में यह मान्यता बढ़ रही है कि स्वस्थ होने के लिए मन और शरीर दोनों का ही स्वस्थ होना आवश्यक है। आयुर्वेद और योग के बारे में जानने की इच्छा दुनियाभर के लोगों को भारत की ओर खींच रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित औषधियों और उपचार पद्धतियों की वैज्ञानिक पुष्टि करना जरूरी है। आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से जड़ी-बूटियों, पंचकर्म और आयुर्वेदिक योगों की प्रभावशीलता को साबित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाओं का वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण इसकी गुणवत्ता मूल्यांकन और वैश्विक स्वीकृति के लिए बहुत आवश्यक है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आयुर्वेद एवं आयुर्वेदिक संस्थानों के हित में, ज्ञान-संवर्धन और ज्ञान के पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु प्रयास करते रहें। आप सभी आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहें एवं स्वस्थ और सबल भारत के ध्येय के प्रति समर्पित रहें, आपसे ऐसी अपेक्षा है।
आपका ज्ञान और आपकी सेवाएं समाज को एक नई दिशा देने में सहायक होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस अमूल्य धरोहर को आत्मसात करें और इसे पूरी दुनिया तक पहुँचाने का संकल्प लें। अंत में, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिन्द,!