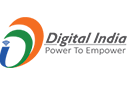12-10-2025:इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के 24वें वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन
जय हिन्द!
आज इस पवित्र देवभूमि उत्तराखण्ड की सुरम्य वादियों में, इस गहन और सार्थक बौद्धिक संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच उपस्थित होकर मैं हृदय से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैं दून विश्वविद्यालय और इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टिट्यूशन (प्।ैैप्) को इस सार्थक और अत्यंत प्रासंगिक तीन दिवसीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूँ।
आज सम्पूर्ण विश्व एक नई दिशा, एक स्थायी समाधान की तलाश में है। वह इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन और असमान विकास जैसी चुनौतियाँ मानव सभ्यता के अस्तित्व तक को गंभीर चुनौती दे रही हैं। ऐसे समय में इस सम्मेलन के विषय “जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चुनौतियाँ, शहरीकरण, सतत विकास और आजीविका संवर्धन” केवल एक अकादमिक विमर्श नहीं, बल्कि हमारी साझी जिम्मेदारी, जागरूकता और सामूहिक चेतना का सशक्त आह्वान है।
ये अहम विषय हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि विकास की दौड़ में हम पृथ्वी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को कितना याद रख पा रहे हैं। साथ ही ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, जहाँ विकास और पर्यावरण दोनों एक-दूसरे के पूरक बनें, प्रतिद्वंद्वी नहीं।
और यह भी अत्यंत अर्थपूर्ण है कि यह सम्मेलन उस पावन भूमि पर आयोजित हो रहा है जिसे “देवभूमि” कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसी यह धरती, जहाँ नदियाँ वेदों का पाठ करती हैं, जहाँ वनों में जीवन की श्वास बसती है, और जहाँ प्रत्येक पर्वत मानवता की करुणा, साहस और अध्यात्म का प्रतीक है। यह भूमि हमें स्मरण कराती है कि प्रकृति और संस्कृति का संतुलन ही सतत विकास का वास्तविक मार्ग है।
प्रकृति से सामंजस्य ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा है। हमारी प्राचीन सभ्यता में पृथ्वी को “भू-माता”, जल को “जीवन का अमृत”, और वनों को “जीवन का आधार” माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का संदेश देकर सम्पूर्ण सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखा। यह दर्शन आज के वैश्विक परिदृश्य में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।
विद्वत साथियों!
हिमालय केवल एक भौगोलिक श्रृंखला नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रीढ़ है। यही वह पर्वत श्रृंखला है, जिसने भारत की सभ्यता को संरक्षण दिया, हमारी नदियों को जीवनदायिनी शक्ति दी, और हमारे मानस को अध्यात्म से जोड़ा।
हमारी नदियाँ केवल जलधाराएँ नहीं हैं, ये भारत की जीवनधाराएँ हैं, जिनसे करोड़ों लोगों का जीवन, उनकी आस्था, उनकी कृषि और उनकी संस्कृति जुड़ी है। जब ये नदियाँ प्रदूषित होती हैं या जब हिमनद पिघलते हैं, तब केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अस्तित्व की निरंतरता भी प्रभावित होती है।
हाल के वर्षों में देश के अनेक पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आए भूस्खलन, अचानक बाढ़ें और चरम मौसमी घटनाएँ हमें बार-बार यह चेतावनी दे रही हैं कि यदि हमने प्रकृति के संतुलन के प्रति अपनी संवेदनशीलता नहीं बढ़ाई, तो इसकी कीमत सम्पूर्ण राष्ट्र को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जब प्रकृति असंतुलित होती है, तो विकास, सुरक्षा और मानवता तीनों खतरे में पड़ जाते हैं।
जलवायु परिवर्तन आज केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। असंतुलित औद्योगीकरण, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध वनों की कटाई, और प्राकृतिक संसाधनों का अति-दोहन – ये सभी इसके मूल कारण हैं।
हम तापमान में लगातार वृद्धि, वर्षा के अनिश्चित पैटर्न, ग्लेशियरों के पिघलने, फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, और वेक्टर जनित रोगों के फैलाव जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।
याद रखिए! पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लोभ को नहीं। इसलिए हमें समझना होगा कि प्रकृति के शोषण से विकास नहीं, विनाश होता है।
इस संकट से निपटने के लिए केवल नीतियाँ या तकनीक पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि हमें जीवनशैली में परिवर्तन, जनसहभागिता, और प्रकृति के प्रति करुणा को अपनी नीति का केंद्र बनाना होगा।
हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए पर्यावरणीय चुनौतियाँ और भी संवेदनशील हैं। भूस्खलन, मृदा क्षरण, नदियों का क्षरण और वन्य जीवों के आवासों में कमी जैसे मुद्दे अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ चुके हैं।
इनसे निपटने के लिए हमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय, जनजागरूकता और शिक्षा, इन तीन स्तंभों पर कार्य करना होगा।
हमें गाँवों और पंचायतों को पर्यावरणीय प्रबंधन में भागीदार बनाना होगा। हमारे पूर्वजों के पर्यावरणीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ना ही इसका सटीक समाधान है। और यह भी आवश्यक है कि पर्यावरणीय चेतना को केवल पाठ्यक्रम नहीं, जीवन मूल्य बनाना होगा।
साथियों,
शहरीकरण आर्थिक विकास का वाहक है, लेकिन अनियोजित शहरीकरण असमानता, प्रदूषण, यातायात और संसाधनों की कमी का कारण भी बन रहा है। शहर यदि पर्यावरण के अनुकूल न हों तो वे अपने ही नागरिकों के जीवन को असुरक्षित बना देते हैं।
हमें “स्मार्ट सिटीज” के साथ-साथ “ग्रीन सिटीज” की भी परिकल्पना करनी होगी, जहाँ भवन ऊर्जा-कुशल हों, परिवहन स्वच्छ हो, और हरित आवरण पर्याप्त हो। “छंजनतम.पदबसनेपअम नतइंद चसंददपदह” ही आने वाले भारत का मॉडल बन सकता है।
सतत विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन है। यह वह दर्शन है जिसमें आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
उत्तराखण्ड जैसे राज्य में, जहाँ प्रकृति ही अर्थव्यवस्था की धुरी है, हमें ग्रीन ग्रोथ, इको-टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारा लक्ष्य “छंजनतम च्वेपजपअम क्मअमसवचउमदज” होना चाहिए। अर्थात् ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए बल्कि उसे सशक्त बनाए।
साथियों,
विकास तब तक अधूरा है जब तक वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक न पहुँचे। सच्चा विकास वही है जो व्यक्ति को सुरक्षा, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन का अवसर दे।
आजीविका संवर्धन केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका, स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास के माध्यम से पलायन की समस्या को रोकना होगा। उत्तराखण्ड के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का हर गाँव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और मानवीय गरिमा का प्रतीक है।
विद्वान जनों,
हिमालय का संरक्षण केवल उत्तराखण्ड की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का दायित्व है। यह क्षेत्र भारत की जल सुरक्षा, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। हमें हिमालय को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं अपितु “स्पअपदह म्बवेलेजमउ” के रूप में देखना होगा।
हमें समझना होगा कि यहाँ के हर वृक्ष, हर झरना, हर बर्फ का कण हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का आधार है। इसलिए हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु एकीकृत नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक सहभागिता और युवाओं की ऊर्जा को जोड़ना आवश्यक है।
मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित हैं। यही युवा हमारे भविष्य के नीति निर्माता, विचारक और परिवर्तनकारी हैं। मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ – “आप केवल भविष्य के विद्यार्थी नहीं हैं, आप भविष्य के निर्माता हैं।” आपके विचार, आपके शोध और आपकी संवेदना ही एक हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा तय करेंगे।
आप सभी ने मिलकर इस सम्मेलन को ज्ञान, संवाद और नीति-चिंतन का एक सुंदर मंच बनाया है। इस गंभीर और सारगर्भित बौद्धिक मंथन के आयोजन के लिए आप सभी की हृदय से प्रसंशा करता हूँ।
मुझे विश्वास है कि यहाँ हुए मंथन से निकले निष्कर्ष नीति निर्माण के स्तर पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेंगे और हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगे।
प्रिय साथियों,
हम सबको मिलकर यह प्रण लेना होगा कि हम केवल प्रकृति के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके संरक्षक बनेंगे। हमें अपनी विकास यात्रा में “प्रकृति के साथ, प्रकृति के लिए और प्रकृति के भीतर” आगे बढ़ना होगा।
आइए! हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ियाँ जब इस धरती को देखें तो कह सकें, ‘‘हमारे पूर्वजों ने धरती को वैसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और सुंदर बनाया।’’
इसी भावना, आशा और अपेक्षा के साथ, मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए पुनः सभी आयोजकों, प्रतिभागियों और विद्वानों को बधाई देता हूँ और सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ।
जय हिन्द!